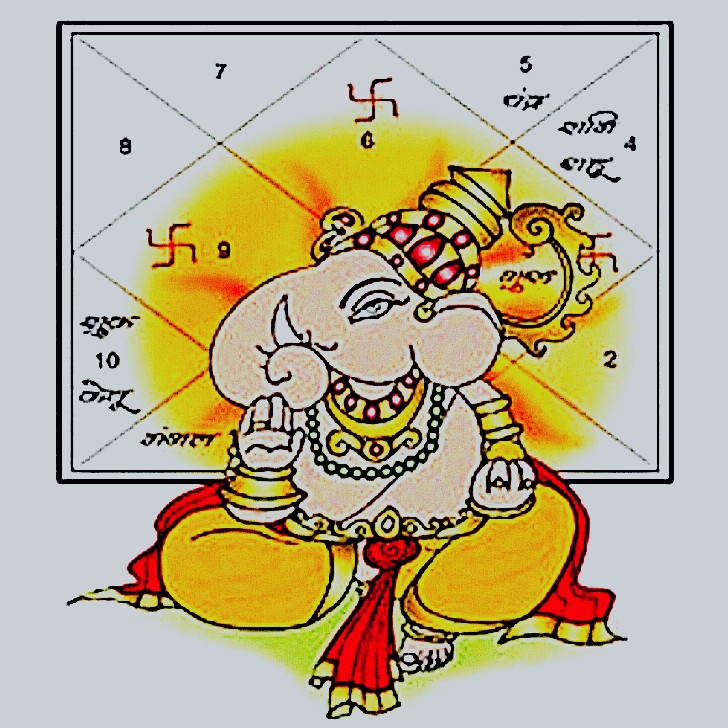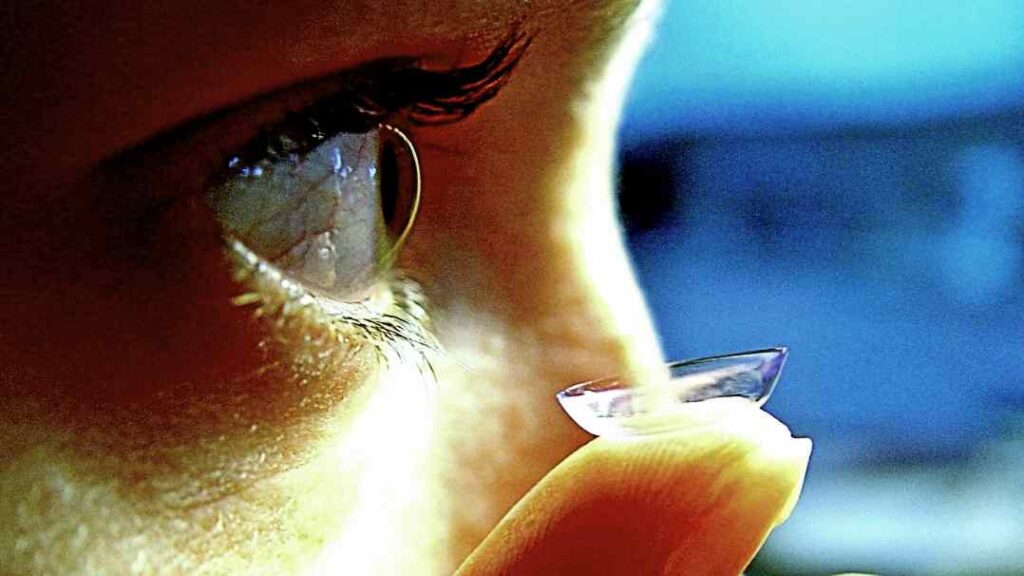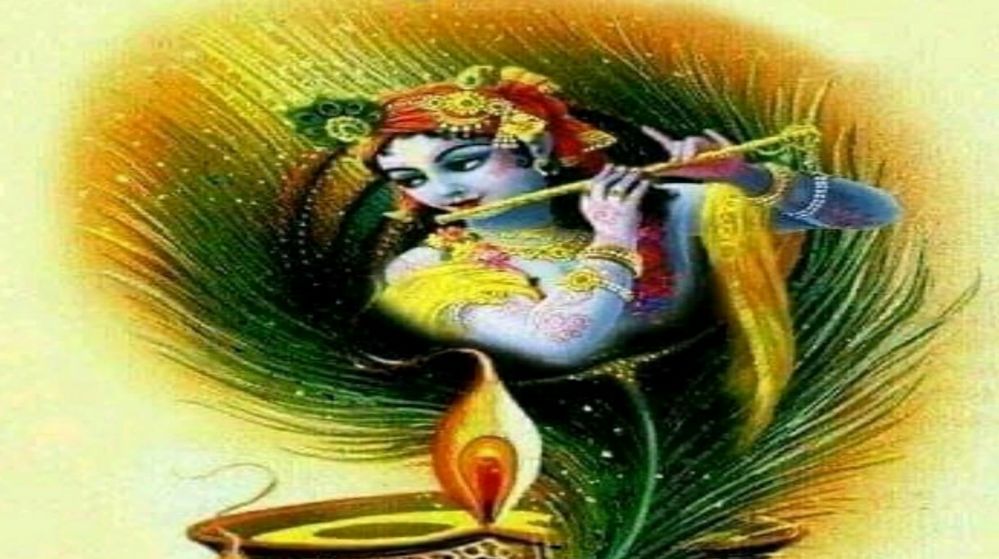प्रश्न कुण्डली- बिना जीवन कुण्डली के जाने
इस लेख के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रश्न कुंडली एक बहुत ही अच्छा तरीका है जब किसी इंसान के पास कुंडली ना हो और उसके पास कोई एक खास सवाल हो तो इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे अच्छा तरीका प्रश्न कुंडली होता है
प्रश्न कुंडली किस तरह काम करती है अगर प्रश्न करने वाला व्यक्ति दिल से ईमानदारी से साफ साफ सवाल पूछता है तो जिस वक्त वह सवाल पूछता है उस वक्त की सभी ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह बनती है कि उनकी वाइब्रेशन उनकी एनर्जी प्रश्नकर्ता के सवाल की एनर्जी के साथ मैच करने लगती है और इसी वजह से प्रश्नकर्ता भी उसी वक्त सवाल करता है।
जब लगन उस सवाल के समकक्ष चल रहा हो इसी वजह से प्रश्न कुंडली हमेशा ऐसे ही बनती है जैसा सवाल पूछा गया है प्रश्न कुंडली में हमेशा सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखा जाता है की लग्नेश और लग्न क्या है, लग्न चर और उसकी दिशा आदि, जो भी बहुत सारी बाते हमने बेसिक एस्ट्रोलॉजी में राशियों के बारे में पढी, वो सभी बाते यहाँ काम आती है।
1• सामान्य प्रश्न विचार :- प्रश्न ज्योतिष से प्रश्न कर्ता जब प्रश्न करता है उसी समय का लग्न बनाकर प्रश्नों का उत्तर दे तो काफी हद तक जो व्यक्ति अभी नया नया ज्योतिष पढ़ रहा हों और ज्यादा अनुभव नहीं भी हों तो भी प्रश्नों का उत्तर निकाल सकता है।
सबसे पहले जब यह निकलना हो उस समय कि कुंडली बना ले | जो भी लग्न चल रहा हों उस लग्न का स्वामी लग्नेश व जिस भाव के लिए प्रश्न किया गया हों वो कार्येष कहलाता है क्रमश: उन दोनों ग्रहों कि जाती, गुण,अवस्था कि जानकारी कर इष्ट फल बताये |
लग्नेश कार्येष अपने अपने भाव में स्थित हों या कार्येष लग्न में हों लग्नेश कार्य भाव में हों तो वांछित सिद्धी मिलती है परन्तु इनमेसे कोई भी एक भाव पर चंद्रमा कि पूर्ण दृष्टि हों तो कार्य पूर्ण रुप से सिद्ध होता है।
अगर एसी स्थिति में इन पर चंद्रमा नहीं देख रहा हों परन्तु और कोई शुभ ग्रह देखता हों तो यह कार्य तो सिद्ध नहीं होगा परन्तु कोई अन्य कार्य कि सिद्धी होगी |
2• प्रश्नकर्ता सीधा है या कुटिल :- लग्न में चंद्रमा व केतु , {१ ४ ७ १० } शनि हों , बुद्ध अस्त हों चंद्रमा मंगल या शनि पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो प्रश्न कर्ता कुटिल है वह ज्योतिषी कि परीक्षा लेने आया है या ज्योतिषी कि मजाक बनाने आया है। जैसा की अक्सर लोग फ्री के नाम पर आते है और ज्योतिषी का वक़्त खराब करते है।
इसलिए आप पृश्नकृता के पृश्न किये बिना भी पृश्न कुंडली बना सकते है। अगर लग्न में शुभ ग्रह हों तो प्रश्नकर्ता सरल व्यक्ति है उसको वाकई अपना भविष्य जानना है |
यदि चंद्रमा , गुरु लग्न या सप्तम स्थान को मित्र दृष्टि से देखते हों तो भी प्रश्नकर्ता सरल स्वभाव का है परन्तु प्रश्न के समय गुरु और चंद्रमा कि शत्रु द्रष्टि सप्तमेश पर हों तो कुटिल है। अगर चंद्रमा व गुरु एक राशी में हों तो प्रश्नकर्ता सरल व्यक्ति है |
3• वर्तमान,भूत या भविष्य कैसा :- यदि चंद्रमा और गुरु का योग सप्तमेश के साथ हों तो प्रश्नकर्ता का वर्तमान समय ठीक है और आगे भी ठीक होगा | यदि ऐसा नहीं है तो वर्तमान भी ठीक नहीं है आगे भी ठीक नहीं होगा |
इसी में लग्नेश व कार्येष का योग जिस दिन हों और कार्येष उदय होकर लग्न में पंहुचे या कार्येष और लग्नेश कि परस्पर दृष्टि हों उसी दिन कार्य होगा | इस तरह से मोटे तोर पर कार्य होगा या नहीं , होगा तो कब होगा यह छोटी छोटी भविष्य वाणी थोड़े से अध्ययन से कि जा सकती है |
मतलब ये सबसे सामान्य नियम है। मेरी आप से विनती है, की आप जब खुद इसकी अभ्यास करेंगे, तो ज्यादा समझ पाएंगे।